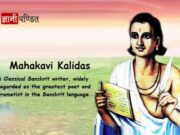कहने को हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो गए, और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक भाग हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अभी लोकतंत्र आया ही नहीं है। लोकतंत्र के आने में अभी कुछ दशक और लग जाएंगे। तब तक हमें राजतंत्र की जरूरत है। यह बुरा लग सकता है कि आजादी का गला घोंटकर मैं राजशाही का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन गौर कीजिए क्या हम छद्म सामंतवाद की छाया में नहीं खड़े हैं। राजशाही (feudalism) में जहां कम से कम एक राजा या सामंत होता है जिसे जिम्मेदार बनाया या बताया जा सकता और व्यवस्था के प्रति भी वही जवाबदेह होता है। वर्तमान भारत में सामंतवादी हरकतें अपने चरम पर हैं, लेकिन कोई राजा या सामंत जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं और सत्ता पर काबिज कुछ लोग, कुछ घराने, धन और ताकत का राज।
क्या वास्तव में हम खुद को धोखे में नहीं रखे हुए हैं। एक नेताजी होते हैं, और उनके पीछे चेलों चपाटों की पूरी फौज। जो उनकी हां में हां मिला रही है। उन नेताजी को कोई बुरा कहने वाला नहीं। अगर कह भी दिया तो नेताजी की मोटी खाल पर कोई असर नहीं। पॉलिटिकल इम्युनिटी (Political immunity) लिए नेता, रावण की तरह हंसते हुए लूटते हैं। यह व्यवस्था कोई बाहर से नहीं आई है।
संसाधन सीमित हैं, उन्हें बढ़ाने का भी कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आजादी (Freedom) के साठ साल बाद शिक्षा का अधिकार दिया गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार तो अब भी कोई जमीनी हकीकत नहीं रखते। पुलिस हमारी सेवा के लिए नहीं बल्कि हमें डंडा दिखाने और भय पैदा करने के लिए है। न्यायालय के बारे में मान लिया गया है कि न्याय में देरी होगी। भले ही यह कहा जाए कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड।
राजनीतिक पार्टियां (political parties) बाहरी ताकतों नहीं लादी हैं। इसी व्यवस्था में शिक्षा और संसाधनों से वंचित लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों का चुनाव किया जो उन क्षेत्रों के लोगों के “काम” आ सके। नतीजा यह हुआ कि काम आने वाला बंदा काम करके ऐसी हैसियत में पहुंच गया कि अपने क्षेत्र में वह शेर है और दूसरी गली में पहुंचते ही दुम दबाए कुत्ता। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक जन नेता तैयार होने की कोई सूरत बाकी नहीं रही।
अब यही क्षेत्रीय लोग मिलकर एक ऐसे नेता का चुनाव करते हैं जो उनके निजी या उनके क्षेत्र के हित साध सके। क्षेत्रीय नेताओं के पास दोहरी चुनौतियां हैं। पहली कि अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखा जाए, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ाए। नेता बदल गया तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाता है। ऐसे में क्षेत्र विशेष की जनता की मजबूरी बन जाती है कि अपने हित साधने के लिए भ्रष्टाचार में डूब चुकने के बाद भी उसी नेता का चुनाव कराए जो पहले से राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कुछ रसूख रखता हो।
इन घटनाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शुरू में एक पार्टी रहती है तो बाद में दूसरी पार्टी लहर के साथ आती है। चूंकि एक पार्टी स्वतंत्रता दिलाने के खम भरते हुए पहले से सत्ता में है सो उसका विघटन भी धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे देश के लोग आजादी की डायलेमा से बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे दूसरी पार्टी को बल मिलता है। आखिर एक लहर आती है और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है।
वही क्षेत्रीय लोग और उसी राज्य और राष्ट्र स्तरीय कमशकश से सामना होता है और दोनों पार्टियों में एक जैसे लोग नजर आने लगते हैं। चूंकि चुनाव खर्चीला है और क्षेत्रीय दबदबा जरूरी चीज है। ऐसे में हर स्तर पर भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है। आखिर में दोनों पार्टियां जॉर्ज ओरवेल के सुअरों जैसी दिखाई देने लगती है।
फिलहाल देश की राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने दम पर सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन का दावा करते हैं। एक हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा के नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) तो दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आप के अरविन्द केजरीवाल (Arvind kejriwal)। दोनों ने अपने अपने तरीके से भारत की जनता में यह छवि बनाने का प्रयास किया है कि चाहे सिस्टम जैसा भी हो, वे अपने दम पर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं।
न तो गुजरात भ्रष्टाचार से अछूता रहा है न दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल इसे मुक्त करा पाए हैं। बस दोनों के पास छवि ही है। इस छवि में ऐसी क्या खास बात है। देखते हैं।
- दोनों अपने दम पर व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हैं
- दोनों खुद को दबंग साबित करते हैं
- दोनों अपने पार्टी पर अपने तरीके की पकड़ रखते हैं
- दोनों के पास सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रभाव डालने की शक्ति है
- दोनों सत्ता पर काबिज पार्टी को हड़काते हैं
- दोनों के पास पर्याप्त धनबल दिखाई देता है
- दोनों के पास जनबल दिखाई देता है
- दोनों के पास अंध भक्तों की लंबी कतार है
एक प्रकार से दोनों जनता की किसी आवाज के बजाय अपनी आवाज अधिक ताकत के साथ जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या एक सामंत यही काम नहीं करता। अगर कोई यह समझने की भूल करे कि वामपंथ में सामंतवाद से लड़ने की शक्ति है तो उन्हें पहले बने यूएसएसआर को देखना चाहिए, जहां हमेशा यह शिकायत रही कि सभी संसाधनों को मास्को में सीमित कर दिया गया है। दूसरी ओर सामंतवाद का सबसे शक्तिशाली उदाहरण खुद चीन है। अगर वहां लोकतंत्र हो तो राजशाही अंदाज में पोलित ब्यूरो की बैठक नहीं होती। हां, कुछ मामलों में यह राजतंत्र से अलग है, लेकिन अंतत: सत्ता और शक्ति को केन्द्रित करने का ही काम करती है। चाहे वह कुछ लोगों के पास हो, एक समूह विशेष के पास हो या एक पूरी संस्था के पास हो।
भारत (India) में ऐसा पोलित ब्यूरो से चलने वाला देश बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए संप्रदायों को दांव पर लगाना पड़ेगा। जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में वामपंथी सामंतवाद को अभी छोड़ दें।
दूसरी ओर लोकतांत्रिक (democracy) सामंतवाद का नतीजा हम 65 सालों से भुगत ही रहे हैं। ऐसे में इस छद्म सामंतवाद को भी विदा करने का वक्त आ गया दिखाई देता है।
तीसरे मिलट्री के हाथ में सत्ता देने का औचित्य दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देश का भूभाग इतना विस्तृत और बेढ़ब है कि मिलट्री द्वारा इसे शासित किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वरना अब तक मिलट्री शासन भी आ सकता था, जैसा पाकिस्तान में आता रहा है।
चौथा सिस्टम वही है असली सामंतवाद। कहने, सुनने और पढ़ने में भले ही बुरा लगे, लेकिन नए जमाने के इस दो राजाओं की टक्कर और उसके बाद के हालात देखने का अलग की कौतुहल होगा। दोनों में से कोई भी आए, अगर ये लोग अपने इस सामंतवादी चोले को छोड़ दें तो अलग बात है, वरना देश में बड़े परिवर्तनों की बयार शुरू हो सकती है। पिछले दस साल से देश ऐसे लुंज पुंज माहौल में आगे बढ़ रहा है, कि विश्व में आई मंदी के दौरान अपनी बचत के जोर से अपने पैरों पर खड़ा देश भी उसका लाभ नहीं उठाया पाया। हमारे लोगों को दुनिया के हर कोने में धमकाया, हड़काया और दबाया जा रहा है।
नए नेतृत्व के बाद कम से कम यह सुकून रहेगा कि पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी है जो किसी भी देश और ताकत को धमकाकर हमें उचित सम्मान दिला सकती है।